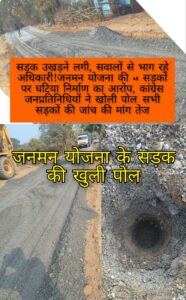“विलुप्त होते मांदर और नगाड़े के बीच लोक जसगीत की परंपरा” संरक्षण की नितांत आवश्यकता।

नवरात्रि का पर्व और छत्तीसगढ़ की परंपरा– आजाद भारत न्यूज़ विशेष रिपोर्ट- प्रदीप शर्मा(प्रधान संपादक)
छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में नवरात्रि पर्व आस्था और उत्सव का प्रतीक है। यहां हर कोने में दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। कई स्थानों पर कलश जोत और जंवारा रखा जाता है। पूरा गांव नौ दिन तक भक्ति में डूबा रहता है।
श्रद्धालु नौ दिनों तक कठिन तप और व्रत का पालन करते हैं। कोई जूते-चप्पल त्याग देता है, कोई मौन व्रत धारण करता है, तो कोई पूरे समय केवल फलाहार पर रहता है। यह सामूहिक अनुशासन और आस्था इस पर्व को खास बनाता है।
जसगीत की अनोखी परंपरा
एक समय था जब नवरात्रि का मतलब था – जसगीत। सुबह, दोपहर और रात तीनों पहर जसगीत होते थे। गांवों में मांदर, नगाड़ा और बांसुरी की ताल पर देवी भक्ति गूंजती थी। ग्रामीण महिलाएं और पुरुष सामूहिक रूप से जसगीत गाते थे, जिससे पूरे वातावरण में भक्ति और आनंद का माहौल छा जाता था।
लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आजाद भारत टीम ने अलग-अलग गांवों का भ्रमण कर पाया कि केवल 10–15 प्रतिशत स्थानों पर ही पारंपरिक वाद्य जैसे मांदर और नगाड़ा सुनाई दिए। वहां भी इन्हें बजाने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग ही थे।


एक बुजुर्ग ने बताया – “पहले जसगीत के बिना नवरात्रि अधूरी लगती थी, अब युवा लोग इसमें रुचि नहीं लेते।”
पीढ़ियों के बीच संवाद का अभाव
बुजुर्ग कहते हैं – “सीख लो, काम आएगा। यह परंपरा तुम्हारे लिए पूंजी है।” लेकिन युवा जवाब देते हैं – “हमें मौका ही नहीं दिया जाता। सिर्फ डांटते हैं, सिखाने का धैर्य नहीं रखते।”
यानी परंपरा खोने के पीछे सबसे बड़ा कारण है – पीढ़ियों के बीच संवाद और सामंजस्य की कमी।
डीजे और आधुनिक धुनों का दबदबा
जहां पहले मांदर-नगाड़े की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब डीजे और साउंड सिस्टम का शोर हावी है। युवा अपने मोबाइल फोन कनेक्ट करके पहले भजन बजाते हैं, फिर थोड़ी देर में फिल्मी गाने और नाच-गाने वाली धुनें चलने लगती हैं।
इस बदलाव ने जसगीत और भजन की गहराई को कमजोर कर दिया है। एक समय की सामूहिक भक्ति अब मनोरंजन और शोरगुल में बदल रही है।
पंडाल सजावट का बदलता स्वरूप
नवरात्रि पंडाल सजाने की परंपरा भी अब बदल चुकी है। पहले ग्रामीण मिलकर लकड़ी, बांस, तिरपाल, बाजवट, गोबर और आम की पत्तियों से पंडाल बनाते थे। इसे बनाने में श्रम, सेवा भाव और सामूहिकता झलकती थी।
कहीं-कहीं रेलवे की पुरानी पटरियों और खाली ड्रमों से मंच तैयार किया जाता था। गांव के युवा समर्पण और उत्साह के साथ यह काम करते थे।
लेकिन अब जगह-जगह टेंट हाउस और तैयार सजावट का चलन हो गया है। पैसे से मिलने वाली सजावट आसान तो है, लेकिन इसमें सेवा-भाव और परंपरा का रंग फीका पड़ गया है।

छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्र
छत्तीसगढ़ अपनी लोक संस्कृति और जनजातीय जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यहां के वाद्य यंत्र केवल संगीत का साधन नहीं, बल्कि पहचान और धरोहर भी हैं।
मांदर – घसिया जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला प्रमुख ढोलक, जिसका प्रयोग सैला और कर्मा नृत्य में होता है।
बांसुरी – पोले बांस से बनी, जिसे हर वर्ग का गायक और वादक प्रयोग करता है।
नगाड़ा – उत्सवों और फाग गीतों में गूंजने वाला भारी वाद्य।
ढोलक – आकार में छोटा, लेकिन शादी-ब्याह और भजनों में खास।
निशान – कमर में पहना जाने वाला ढोल, जो लोहे और चमड़े से बनता है।
तुरही – बस्तर की पहचान, शहनाई से बड़ा और उत्सवों में प्रयोग होने वाला वाद्य।
अलगोजा – बांसुरी जैसा, जिसे मेलों और मड़ई में बजाया जाता है।
इनके अलावा चीकारा (सारंगी), मोहरी-शहनाई, ताशा, और खंजरी-कठताल भी परंपरागत वाद्य यंत्र हैं।

संस्कृति बचाने की जरूरत
आज जसगीत और पारंपरिक वाद्यों का लोप केवल एक परंपरा का खोना नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का कमजोर होना है।
जरूरत है कि –
1. बुजुर्ग युवाओं को मौका दें और धैर्य से सिखाएं।
2. विद्यालयों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पारंपरिक वाद्यों का प्रशिक्षण शुरू हो।
3. गांव समितियां डीजे पर निर्भरता कम करें और जसगीत व भजन को प्राथमिकता दें।
4. युवाओं को मंच पर उतारा जाए ताकि वे सीखने और निभाने का आत्मविश्वास पा सकें।
अगर आज कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मांदर और नगाड़ा सिर्फ संग्रहालय की चीज बनकर रह जाएंगे।
प्रदीप शर्मा (प्रधान संपादक- आजाद भारत न्यूज़)
![]()